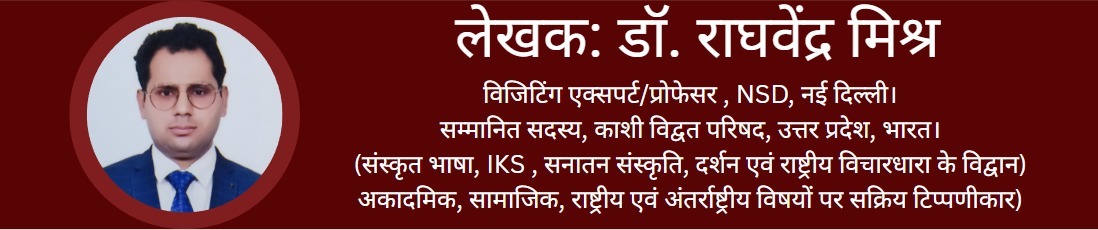यह लेख भारतीय नृत्य परंपरा के विकास को भरतमुनि के नाट्यशास्त्र को आधार बनाकर दो चरणों में विश्लेषित करता है नाट्यशास्त्र के पूर्व एवं पश्चात्। वैदिक, पौराणिक, आगमिक तथा लोक परंपराओं में व्याप्त नृत्य के प्रारंभिक स्वरूपों से लेकर नाट्यशास्त्र द्वारा शास्त्रीय अनुशासन प्राप्त नृत्य संरचनाओं तक का समग्र अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। यह शोध नृत्य को भारतीय ज्ञान परंपरा में आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टियों से जोड़ता है।
प्रस्तावना:
भारतीय नृत्य परंपरा, एक कला मात्र नहीं, अपितु एक जीवनशैली, धर्मानुष्ठान और सांस्कृतिक संवाद का माध्यम है। नाट्यशास्त्र की रचना ने इस परंपरा को एक शास्त्र रूप प्रदान किया, जिससे पूर्व की बिखरी हुई नृत्य परंपराएं एक संगठित और व्याख्यायित रूप में परिवर्तित हो गईं।
नाट्यशास्त्र के पूर्व की नृत्य परंपराएँ
वैदिक और उपनिषदकालीन परंपरा
ऋग्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद में नृत्य का उल्लेख यज्ञों, उत्सवों और देवताओं की आराधना के रूप में होता है। ऋग्वेद के मंत्रों में "नृत्य" शब्द का प्रयोग हुआ है, जैसे “नृत्यद्वाजं रथेष्ठां वृषणं हुवे”। श्वेताश्वतर उपनिषद में ईश्वर को नृत्य करते हुए मुनियों में देखा गया है "नृत्यते मुनिः आत्मन्येव"।
पौराणिक व आगमिक नृत्य दृष्टि
शिव के ताण्डव और पार्वती के लास्य से नृत्य के द्वैत भाव की स्थापना होती है। विष्णु के रासलीला रूप में भक्ति रस प्रधान नृत्य की कल्पना दिखाई देती है। लिंगपुराण, शिवपुराण, नारद पुराण में नृत्य को ब्रह्मांडीय ऊर्जा और धर्म का अवयव माना गया है।
लोक परंपराएँ

भील, संथाल, गोंड, यक्षगान, छाऊ जैसे नृत्य लोक जीवन से सीधे जुड़े रहे। इनकी भाषा, संगीत, ताल, वेशभूषा और भाव प्रदर्शन स्थानीयता में निहित थी। ये नृत्य उत्सव, युद्ध, विवाह तथा देवी-देवता की पूजा से संबद्ध होते थे।
नाट्यशास्त्र का आगमन: नृत्य की शास्त्रीय संरचना
नाट्यशास्त्र में अंगिक, वाचिक, सात्त्विक, और आहार्य अभिनय के साथ नृत्य की व्यापक परिभाषा दी गई। रस-सिद्धांत, भाव, चारी, करण, अंगहार, तथा नृत्त-नृत्य-नाट्य की स्पष्ट व्याख्या की गई। शिव के 108 करणों का उल्लेख – जो शास्त्रीय नृत्य की मूल इकाई बने।
भरतमुनि ने नृत्य को तीन भागों में विभाजित किया:
नृत्त – शुद्ध गति और चालनाएँ
नृत्य – भावप्रदर्शन सहित गति
नाट्य – संवाद और अभिनयप्रधान नाट्य
इसके साथ ही रस सिद्धांत के आधार पर नृत्य को दर्शक के हृदय में अनुभवजगत की अनुभूति कराने वाला माध्यम माना गया।
नाट्यशास्त्र के पश्चात् विकसित नृत्य परंपराएँ
नृत्य की क्षेत्रीय शाखाएँ
नाट्यशास्त्र के पश्चात् भारत में नृत्य विभिन्न शैलियों में विभाजित होकर समृद्ध होता गया:
भरतनाट्यम् (तमिलनाडु) – मंदिर-नृत्य, देवदासी परंपरा, अभिनय और करणा प्रधान
कथक (उत्तर भारत) – कथा वाचन से उत्पन्न, दरबारी और लोक दोनों प्रभाव
ओडिसी (ओडिशा) – त्रिभंगी, चौक, जगन्नाथ मंदिर परंपरा
मणिपुरी (मणिपुर) – रासलीला आधारित, माधुर्य रस
कथकली (केरल) – वीर रस, रंगमंचीय, मुखाभिनय पर केंद्रित
कुचिपुड़ी (आंध्रप्रदेश) – नाट्य रूप में नृत्य
सत्रिया (असम) – वैष्णव भक्ति पर आधारित, शंकरदेव द्वारा प्रस्थापित
ग्रंथ परंपरा
नंदिकेश्वर – अभिनयदर्पण
शारंगदेव – संगीतरत्नाकर
अभिनवगुप्त – अभिनवभारती (नाट्यशास्त्र पर टीका, रस की अनुभूति को केंद्रीय स्थान)
तुलनात्मक विश्लेषण
पक्ष नाट्यशास्त्र से पूर्व नाट्यशास्त्र के पश्चात
दृष्टिकोण धार्मिक, अनगढ़ कलात्मक, शास्त्रबद्ध
विधि लोक प्रेरित, परंपरागत अनुशासित, ग्रंथाधारित
सौंदर्यशास्त्र प्राकृतिक सांख्यिक, दार्शनिक
भाव सामूहिक आस्था व्यक्तिगत अनुभूति
प्रयोजन आराधना, अनुष्ठान सौंदर्य, संवाद, साधना
निष्कर्ष
भारतीय नृत्य परंपरा का इतिहास केवल एक कलात्मक अनुशासन का इतिहास नहीं, बल्कि भारत के धार्मिक, सामाजिक और दार्शनिक चिंतन की गूढ़तम अभिव्यक्ति है। नाट्यशास्त्र ने इस परंपरा को एक शास्त्रीय आधार, तात्त्विक गहराई और सार्वकालिकता प्रदान की। यह स्पष्ट है कि नृत्य भारत में केवल देह की गति नहीं, बल्कि आत्मा की गति है "नृत्यते आत्मा प्रबुद्धः।"
ग्रंथ और संदर्भ सूची
Natyashastra of Bharata, Translated by Manomohan Ghosh, Asiatic Society
Abhinavabharati by Abhinavagupta
Abhinaya Darpanam – Nandikeshwara
Sangeet Ratnakar – Sharngadeva
Kapila Vatsyayan – Traditions of Indian Classical Dance
Raghavan, V. – Bharata’s Natyashastra and Its Tradition
Reports and Papers from Sangeet Natak Akademi and IGNCA.